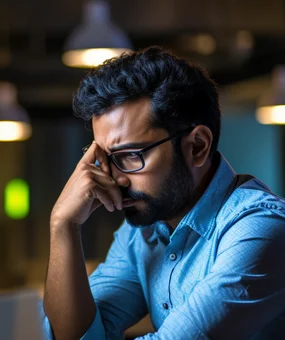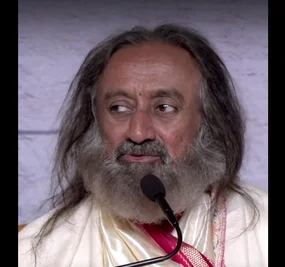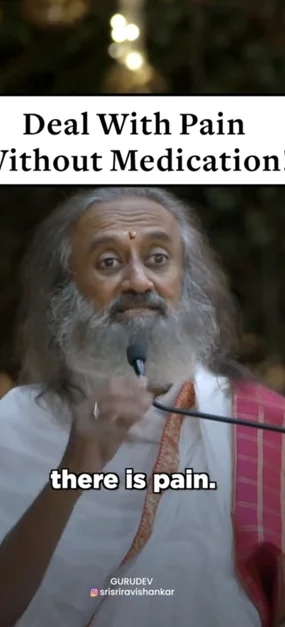जीवन में दुःख के मूल कारण क्या हैं?
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः॥३॥
अविधा, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यही पाँच क्लेश हैं।
अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्॥४॥
अविद्या
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या॥५॥
अविद्या दुःख का एक मूल कारण है, अविद्या क्या है?
जो नित्य नहीं है उसे नित्य मानना अविद्या है। जो बदल रहा है उसे स्थायी मान लेना अविद्या है। जो आनंद नहीं है उसे आनंद मान लेना, जो आत्म नहीं है उसे आत्म मान लेना अविद्या है। मैं शरीर नहीं हूँ पर मुझे शरीर मान लेना ही अविद्या है। मैं विचार और भावना भी नहीं हूँ पर मैं ऐसे मान लूँ की मेरे विचार और मेरी भावनाएँ ही मैं हूँ, यही अविद्या है।
इस शरीर को भी स्थिर मान लेना अविद्या है क्योंकि शरीर तो निरंतर बदल रहा है। नित प्रतिदिन तुम्हारा शरीर बदल रहा है, हर चौबीस घंटे में तुम्हारे भीतर खून बदलता ही रहता है। हर पाँच दिन में तुम्हारे पेट की परत बदल जाती है। एक महीने में त्वचा बदल जाती है। एक वर्ष में शरीर की सभी कोशिकाएँ बदल जाती हैं। तुम इस शरीर को एक नदी के जैसे भी समझ सकते हो, यह निरंतर ही बदलता रहता है। तीन वर्ष में तो पूरा शरीर ही नया हो जाता है। जैसे ही तुम्हें यह बात समझ आती है कि मन भी बदल रहा है तब तुम अपने आप को पुराने विचारों, चिंताओं और भय से अलग देख पाते हो। भूतकाल को पकड़ के रखना अविद्या है, उसे सत्य मान कर बैठ जाना अविद्या है।
अपने आप के बारे में एक धारणा बना कर रखना, कि मैं ऐसा हूँ, यह सब अविद्या है। लोग सोचते हैं कि अपने बारे में जानना एक बड़ी बात है, अरे जिस दिन तुम अपने बारे में एक धारणा निश्चित कर लेते हो, फिर बस, उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम उसमें अटक जाते हो। तुम्हें यह न पता हो कि तुम कौन हो, वही ठीक दृष्टिकोण है। तुम हर क्षण बदल रहे हो और तुम आगे भी बदलाव की संभावना को बनाये रखते हो, वह श्रेष्ठ है।
तुम्हारी अपने बारे में एक निश्चित धारणा तुम्हें पूरी तरह तबाह कर देती है, तुम्हारे विकास में बाधक होती है और सभी संभावनाओं को सीमित कर देती है।
अस्मिता
दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता॥६॥
अपनी बुद्धि को ही स्वयं से एकरूप समझना अस्मिता है। कुछ लोगों के साथ तुमने यह देखा होगा की वह कुछ बात बोलेंगे और बार बार उसी को दोहराते रहेंगे। इस तरह अपनी किसी बात पर अड़े रह कर लगातार तर्क करते जाते हैं, उनके तर्कों में भी कोई तुक नहीं होती। ऐसे अर्थहीन तर्क इसलिए उठते हैं क्योंकि वे लोग अपनी बुद्धि को ही स्वयं का स्वरुप समझ बैठे हैं। इस प्रकार बुद्धि, मन और किसी विचार में अटक जाना अस्मिता है।
स्वयं, बुद्धि और अनुभव के लिए प्रयुक्त इन्द्रियों को पृथक-पृथक न देख पाना अस्मिता है।
राग
सुखानुशयी रागः॥७॥
राग हमेशा किसी अच्छे अनुभव के ही प्रति होता है। कोई भी तुम्हारा अच्छा अनुभव, तुम्हारे अंदर तृष्णा ले आता है। इस तृष्णा या तीव्र इच्छा के कारण तुम दुखी हो जाते हो।
द्वेष
दुःखानुशयी द्वेषः॥८॥
द्वेष अर्थात घृणा, द्वेष किसी भी अप्रिय अनुभव के साथ आता है। द्वेष भी वैसे ही दुःख लेकर आता है जैसे किसी सुखद अनुभव के लिए तृष्णा। राग और द्वेष दोनों ही दुखदायी हैं।
अभिनिवेश
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः॥९॥
अभिनिवेश अर्थात भय, ऐसा प्रायः देखा गया है कि तुम्हें बुद्धि के स्तर पर तो बहुत कुछ पता होगा पर फिर भी कहीं न कहीं भय बना रहता है। तुम बहुत पढ़े हुए हो, ज्ञानी हो, फिर भी कुछ न कुछ भय बना ही रहता है।
महृषि पतंजलि ने यह बड़ी सुन्दर व्याख्या की है। इन पाँच के अतिरिक्त दुःख का कोई और छठा स्त्रोत होना संभव ही नहीं है। अविद्या में जब हम बदलते हुए को स्थिर मान लेते हैं तब हम दूसरों के मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यह ऐसा होना चाहिए, यह वैसे होना चाहिए पर यह संभव है क्या? किसी को तुमसे कल प्रेम था आज नहीं है, क्या पता, वह स्वयं ही अपने मन का कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम यह समझ रहे हो?
तुम संसार में हर किसी से आत्मज्ञानी जैसे व्यवहार की आशा करते हो और तब तुम दुखी हो जाते हो। तुम स्वयं आत्मज्ञानी जैसे व्यवहार नहीं करते हो पर सभी से आत्मज्ञानियों के जैसे व्यवहार और निःस्वार्थ प्रेम की आकांक्षा रखते हो। कई लाखों में एक होगा जो तुम्हें बिना शर्त प्रेम करेगा, यदि तुम वैसा ही प्रेम सबसे चाहोगे तो दुखी हो ही जाओगे। जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, हर व्यक्ति यही कर रहा है, हर व्यक्ति सामान्य लोगों से बिना शर्त के प्रेम चाहता है जैसा उन्हें मुझसे मिलता है। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वे किस बात की इच्छा पाल कर बैठे हैं और वह कितनी बड़ी इच्छा है। तुम हर व्यक्ति में ईश्वर तलाश रहे हो और इस बात से अनभिज्ञ हो कि ईश्वर किसी भी तरह से व्यवहार कर सकता है। तुम अपने आसपास के लोगों में किसी संत स्वरूप ईश्वर को ढूंढ रहे हो। व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति ऐसे नहीं वैसे होनी चाहिए, यह बात तुम्हें दुखी कर देती है।
प्रकृति ने यह पाँच क्लेश हर शरीर के साथ दिए ही हैं। अब प्रश्न यह है कि इनकी परत को कितना क्षीण किया जा सकता है और यह कितनी मोटी बनी रह सकती है। यही तुम्हें जीवन में परिष्कृत या अपरिष्कृत बनाता है।